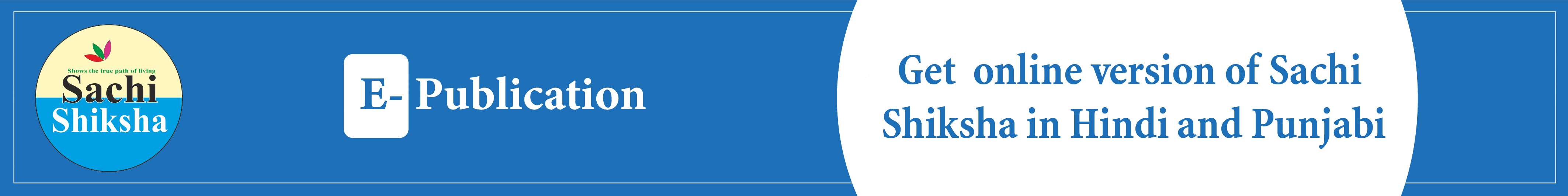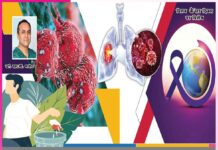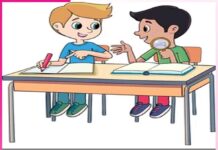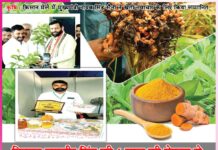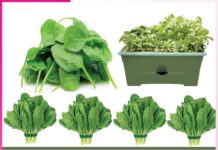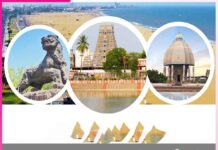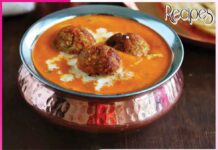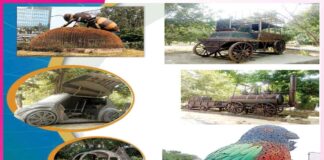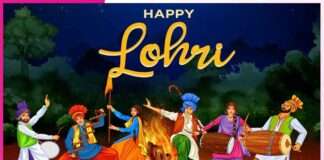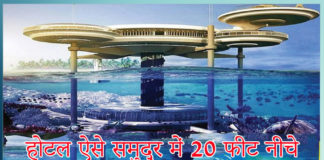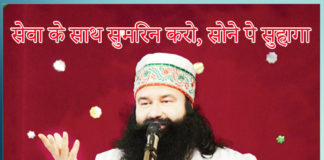सांसों की डोर को मजबूत बनाता है -प्राणायाम
योग के आठों अंगों में प्राणायाम सबसे प्रमुख अंग है। प्राण को विकसित करने वाली प्रणाली का नाम ही ’प्राणायाम‘ होता है। मानव का अस्तित्व इसी प्राण के कारण होता है। इसके बिना हम जीवित रहने की कल्पना तक नहीं कर सकते। जब हम स्वाभाविक रूप से श्वास लेते हैं तो वह जीवनी शक्ति को सामान्य तो बनाए रखती है परन्तु वह उसे विकसित नहीं कर पाती। जब हम अस्वाभाविक रूप से या जल्दी-जल्दी या अधूरी श्वास लेते हैं तो हमारी जीवनी शक्ति क्षीण होती है, साथ ही मुंह से या नाक से अशुद्ध वायु को भी ग्रहण करते रहते हैं जो शरीर पर काफी बुरा प्रभाव डालती है।
जब बच्चा जन्म लेता है तो वह श्वास लेने की पद्धति को जानता है, क्योंकि उसे प्रकृति मदद करती है। इससे बच्चे की जीवन शक्ति मजबूत बनी रहती है और रोग का आक्र मण जल्दी नहीं हो पाता। बचपन में बच्चा पेट से श्वास लेता है जिसे ’पूर्ण यौगिक श्वसन‘ कहा जाता है। इसमें आॅक्सीजन की पूरी मात्रा शरीर में जाती है। ज्यों-ज्यों हम बड़े होते जाते हैं, त्यों-त्यों हम प्रकृति से दूर होते चले जाते हैं। नतीजतन हम अनेक रोगों की गिरफ्त में फंसते चले जाते हैं।

हमारे पूर्वजों ने जंगलों में रहकर अनेक वर्षों तक तपस्या करने के बाद ’प्राणायाम‘ रूपी संजीवनी को खोज निकाला। उन्होंने अपने विस्तृत अध्ययनों में पाया कि मनुष्यों की अपेक्षा जानवर कम श्वास छोड़ते हैं, इसी कारण वे दीर्घजीवी होते हैं। अगर श्वास धीमी चलती है तो हृदय की गति भी कम होती है, जिससे वे लंबी उम्र तक जीवित रहते हैं। जब श्वास अधिक तेजी से चलता है तो हृदय की धड़कन भी तेज चलती है जिससे आयु कम हो जाती है।
योगशास्त्र में प्राणायाम की अनेक विधियां बतायी गयी हैं जिनमें पूरक, रेचक तथा कुम्भक विधियां मुख्य मानी जाती हैं। पूरक का अर्थ होता है श्वास को भरना और रेचक का अर्थ है श्वास को बाहर निकालना। इसी प्रकार कुम्भक का अर्थ होता है-श्वास को रोककर रखना। श्वास को रोककर रखने की प्रणाली ही दीर्घ जीवन को प्रदान करती है।
प्राणायाम से फेफड़ों को शक्ति मिलती है तथा उन्हें अधिक लचीलापन प्राप्त होता है। इससे पूरे शरीर में आॅक्सीजन का संचरण होने लगता है तथा शरीर का प्रत्येक अंग पुष्ट व निरोग होने लगता है। इससे शरीर के अंदर की दूषित वायु बाहर निकलती रहती है। प्राणायाम के समय रक्त परिभ्रमण में तेजी आ जाती है जिससे रक्त मस्तिष्क की सूक्ष्म नाड़ियों तक आसानी से पहुंच जाता है। इससे शरीर सम्पूर्ण दिन तरोताजा रहता है।
प्राणायाम का अभ्यास हमेशा खुली हवा में बैठकर ही करना चाहिए। पद्मासन, वज्रासन अथवा सिद्धासन में ही बैठकर प्राणायाम करना उचित होता है। इसका अभ्यास नियमित रूप से तीन से पांच मिनटों तक ही करना चाहिए। बाद में धीरे-धीरे इसकी अवधि बढ़ायी जा सकती है।
प्राणायाम की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि मादक पदार्थों का सेवन न किया जाये। इसे प्रात:काल शौच आदि से निवृत्त होने के बाद ही करना चाहिए। प्राणायाम की शुरूआत के लिए शरद ऋतु सबसे उत्तम ऋतु मानी जाती है। प्राणायाम के समय शरीर स्थिर तथा सीधा रखना आवश्यक होता है। प्राणायाम सांसों की डोर को मजबूत बनाने का एक सरल एवं उत्तम साधन माना जाता है।
आनंद कु. अनंत